आज का भारत एक ओर “विश्वगुरु” बनने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर उसके सबसे बड़े संसाधन — युवा वर्ग — खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शिक्षा, जो कभी विकास की सीढ़ी मानी जाती थी, आज युवाओं के लिए बेरोजगारी और शोषण का माध्यम बन चुकी है। संविदा पर आधारित रोज़गार न केवल अस्थिरता को जन्म देता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक तौर पर भी युवा वर्ग को तोड़ता जा रहा है।
बेरोजगारी – आंकड़ों से परे एक सच्चाई
भारत में हर साल लाखों युवा स्नातक, परास्नातक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर निकलते हैं, लेकिन नौकरियाँ नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 7.8% के आसपास रही, लेकिन ग्रामीण और शिक्षित युवाओं के बीच यह आंकड़ा कहीं अधिक भयावह है।
- बेरोजगारी अब सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं रही, यह मानसिक अवसाद और सामाजिक उपेक्षा की बड़ी वजह बन रही है।
- खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में शिक्षित युवाओं को न तो स्थायी सरकारी नौकरी मिलती है, और न ही प्राइवेट सेक्टर में स्थिरता।
संविदा प्रणाली – आधुनिक दौर की गुलामी?
सरकारी संस्थान आजकल स्थायी कर्मचारियों की जगह संविदा (contract-based) कर्मियों को नियुक्त कर रहे हैं। इसका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ रहा है जो वर्षों की पढ़ाई और प्रशिक्षण के बाद नौकरी पाते हैं — पर सिर्फ नाम के लिए।
उत्तर प्रदेश का उदाहरण:
- अनुदेशक (Instructor): पिछले 12 वर्षों से कार्यरत, लेकिन वेतन मात्र ₹7,000–₹9,000 प्रति माह
- शिक्षामित्र: वर्षों तक शिक्षक जैसे कार्य, लेकिन मानदेय केवल ₹10,000 प्रति माह, और पिछले 8 वर्षों से स्थायीत्व की कोई उम्मीद नहीं
क्या यही विकास का मॉडल है, जहां शिक्षकों से कार्य तो पूरे शिक्षक जैसा लिया जाता है, लेकिन उन्हें सिर्फ “स्वीकृति” के नाम पर ज़लील किया जाता है?
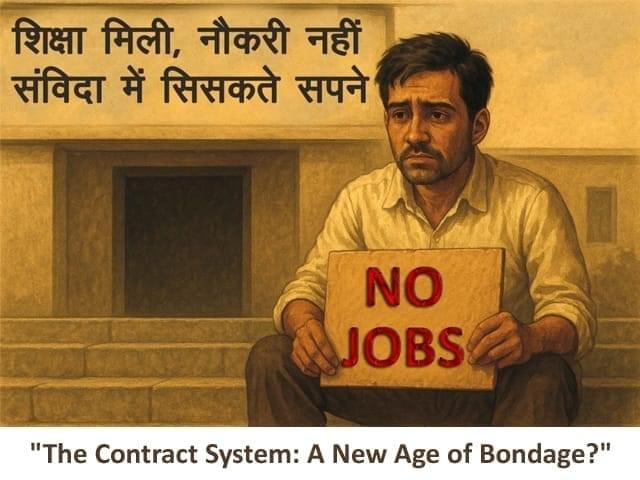
युवाओं के लिए शिक्षा एक छलावा
आज का युवा पढ़ता है, कोचिंग करता है, प्रतियोगी परीक्षाएं देता है — लेकिन परिणामस्वरूप या तो वेटिंग लिस्ट में फंसा रहता है, या फिर संविदा जैसे असुरक्षित मॉडल में फंस जाता है।
- इन युवाओं का भविष्य अधर में लटका रहता है
- समाज उन्हें एक ‘अस्थायी कर्मचारी’ की नजर से देखता है
- विवाह, सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास — सब कुछ प्रभावित होता है
राजनीतिक चुप्पी और जिम्मेदारी से बचाव
हर सरकार यह कहकर बच निकलती है कि “ये समस्या पिछली सरकार की देन है।” लेकिन सवाल यह है कि:
- अगर हर सरकार सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों को दोष देगी, तो फिर वर्तमान की ज़िम्मेदारी कौन लेगा?
- किसने अनुदेशकों को स्थायी करने के वादे किए थे?
- किसने शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने की घोषणाएं की थीं?
राजनीति सिर्फ वादों और घोषणाओं तक सीमित रह गई है। ज़मीन पर संविदाकर्मियों को केवल प्रलोभन और असुरक्षा ही मिली है।
आत्महत्या – एक चुप्पी जो चीख बन चुकी है
वेतन की अस्थिरता, सामाजिक अपमान, और भविष्य की अनिश्चितता के कारण संविदाकर्मी आत्महत्या की ओर मजबूर हो रहे हैं।
उदाहरण:
- 2023 में प्रयागराज जिले के एक अनुदेशक ने आत्महत्या की — उसका आखिरी नोट था: “घर कैसे चलाऊँ?”
- कई शिक्षामित्रों ने परिवार के दबाव, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक तिरस्कार के चलते जान दी
यह एक नैतिक प्रश्न है — क्या एक संवैधानिक राज्य में ऐसे हालात किसी के लिए स्वीकार्य हैं?
समाधान की दिशा में संभावनाएं
संविदाकर्मियों का स्थायीत्व:
सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए जिससे 10 वर्षों से अधिक सेवा दे चुके कर्मियों को स्थायी किया जा सके।
मानदेय की समीक्षा:
वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए ₹10,000 या ₹9,000 की राशि अपमानजनक है। यह कम-से-कम ₹35,000 तक की जानी चाहिए।
राजनीतिक इच्छाशक्ति:
जब वोटों के लिए आरक्षण की नीति बदली जा सकती है, तो रोजगार और सेवा शर्तों में सुधार क्यों नहीं?
न्यायिक हस्तक्षेप:
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इन मामलों को स्वतः संज्ञान में लेकर श्रमिकों के हक की रक्षा करनी चाहिए।
सामाजिक जागरूकता:
समाज को संविदाकर्मियों को ‘नौकर’ नहीं, श्रमवीर के रूप में देखना होगा।
युवा सिर्फ आँकड़ा नहीं, देश का भविष्य है
देश का युवा जब शिक्षित होकर भी बेरोजगार या शोषित होता है, तो वह भविष्य के प्रति आशा नहीं, घृणा और अवसाद पालता है।
अगर हम सच में ‘न्यू इंडिया’ या ‘विकसित भारत’ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने शिक्षित युवाओं और संविदा कर्मियों को सम्मान और सुरक्षा देना होगा।
आज सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है — सवाल विश्वास और उम्मीद का है।
और अगर यही उम्मीद टूटी, तो समाज और व्यवस्था दोनों खोखली हो जाएँगी।
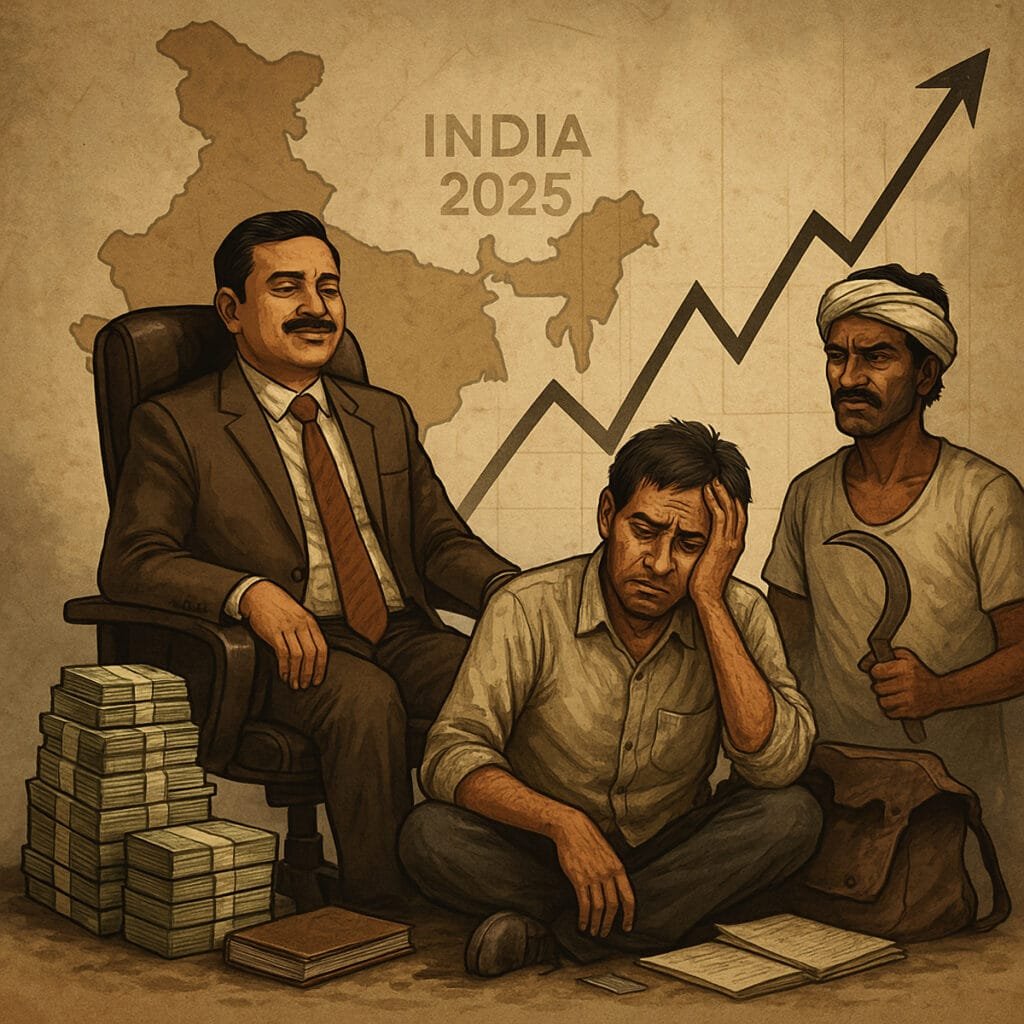
सपनों की संविदा
पढ़-लिख के हम बैठे हैं, हाथों में बस फ़ॉर्म लिए,
सरकारी वादे सुनते-सुनते, अरमान सारे थक से गए।
हर महीने दो वक़्त की रोटी भी अब सपना लगती है,
संविदा में जीवन बीत रहा, पर नौकरी अब भी अजनबी सी लगती है।
अनुदेशक हों या शिक्षामित्र, सबकी एक ही कहानी है,
कभी अपमान, कभी कुंठा – ये रोज़ की रवानी है।
शोषण सहते, चुप रहते, फिर भी उम्मीद जिंदा है,
क्या कभी सुनेगा कोई, जो वाकई ज़िम्मेदार है?
सरकारी नीतियों का खेल
काग़ज़ों में सब ठीक है, फ़ाइलों में योजनाएँ हैं,
जमीं पर देखो हाल तो, बस टूटी उम्मीदें और गालियाँ हैं।
विकास के पोस्टर चमकते हैं, भाषणों में जयघोष है,
पर बेरोज़गार की झोली में अब भी केवल रोष है।
संविदा का नाम देके, सस्ते में काम कराते हैं,
फिर वादों की चाशनी में, जख्मों को भी सहलाते हैं।
नीतियाँ बनती सत्ता के हित में, जनता बस गिनती है,
जिसका हक़ है नौकरी पाने का, वो आज खुद बिकती है।





“Unemployment isn’t just a lack of work—it’s a loss of dignity, direction, and hope. Solving it means more than creating jobs; it means restoring lives.”