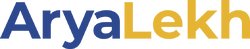लोकतंत्र का मूल भाव “जनता के लिए, जनता द्वारा, और जनता का शासन” होता है। परंतु जब संस्थाएं निष्क्रिय, मीडिया पक्षपाती, विपक्ष मौन और जनता उदासीन हो जाए, तो यह पूछना जरूरी हो जाता है — यदि लोकतंत्र खतरे में है, तो जिम्मेदार कौन है?
इस लेख में हम लोकतंत्र पर मंडराते खतरों का विश्लेषण करेंगे, उन कारणों को खोजेंगे जो इसकी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, और उन संभावित समाधानों की चर्चा करेंगे जो इसे फिर से सशक्त बना सकते हैं।
I. लोकतंत्र के चार स्तंभ और उनकी स्थिति
1. विधायिका:
- विधायिका का कार्य है जनहित में कानून बनाना और सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। परंतु कई बार सत्रों की कार्यवाही बाधित होती है, विधायकों का बहुमत केवल दलगत राजनीति पर निर्भर होता है।
- उदाहरण: हाल के वर्षों में संसद में चर्चा की बजाय अध्यादेशों का प्रयोग बढ़ा है।
2. कार्यपालिका:
- शासन की सभी क्रियाएं इसी स्तंभ से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब ये सत्ता के दबाव में पक्षपाती निर्णय लेने लगे, तब विश्वास कम होता है।
- उदाहरण: सरकारी एजेंसियों जैसे CBI, ED का प्रयोग विपक्षी नेताओं के विरुद्ध चुनिंदा रूप से होना।
3. न्यायपालिका:
- लोकतंत्र की रक्षा की अंतिम दीवार न्यायपालिका है। लेकिन इसके निर्णयों में भी विलंब और पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं।
- उदाहरण: संवेदनशील मामलों में वर्षों तक सुनवाई न होना, जैसे चुनाव सुधार या EVM पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे।
4. मीडिया:
- मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, परंतु कॉर्पोरेट स्वामित्व और TRP की होड़ ने इसे ‘गोदी मीडिया’ की छवि दे दी है।
- उदाहरण: किसानों के आंदोलन में मीडिया का दोहरा रवैया — एक तरफ सरकारी पक्ष, दूसरी तरफ आंदोलन को ‘खालिस्तानी’ कहने वाला नैरेटिव।

“Protesters hold placards and raise slogans during a demonstration against the Citizenship Amendment Act (CAA) and NRC, symbolizing the spirit of democratic dissent in India.” — “लोकतांत्रिक विरोध की भावना का प्रतीक।”
Image Source: AFP via Al Jazeera, December 2019
II. जनता की भूमिका और उदासीनता
1. नागरिकों का मौन:
- जब नागरिक सवाल करना छोड़ दें, जब जन आंदोलनों में हिस्सेदारी घट जाए, तब लोकतंत्र कमजोर होता है।
- उदाहरण: चुनावों में कम मतदान प्रतिशत, खासकर शहरी क्षेत्रों में।
2. धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण:
- सत्ताधारी दलों द्वारा भावनात्मक मुद्दों को उभारकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना।
- उदाहरण: रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बहस की बजाय मंदिर-मस्जिद की राजनीति।
3. शिक्षा और राजनीतिक साक्षरता का अभाव:
- लोगों को नहीं मालूम कि संविधान क्या अधिकार देता है, या किस प्रतिनिधि से क्या अपेक्षा की जानी चाहिए।
- NCERT की 2022 रिपोर्ट के अनुसार 70% छात्र पंचायत से लेकर संसद तक की संरचना से अनभिज्ञ हैं।
III. लोकतंत्र पर मंडराते वर्तमान खतरे
1. संस्थाओं की स्वतंत्रता पर आघात
- चुनाव आयोग, विश्वविद्यालय, न्यायिक नियुक्ति जैसी संस्थाएं सरकार के दबाव में आती दिखती हैं।
- उदाहरण: कुलपतियों की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप कई राज्यों में सामने आए हैं।
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण
- विरोधी विचार रखने वालों को देशद्रोही, टूलकिट गैंग जैसे नामों से बदनाम करना।
- उदाहरण: 2020–2023 के बीच सोशल मीडिया पोस्ट पर 750+ केस दर्ज हुए।
- कला और संस्कृति: फिल्मों, पुस्तकों और थिएटर पर प्रतिबंध और सेंसरशिप बढ़ी है।
3. डिजिटल निगरानी और डेटा नियंत्रण
- Pegasus स्पाइवेयर के माध्यम से 300+ पत्रकार, एक्टिविस्ट्स और नेताओं की निगरानी हुई।
- डेटा सुरक्षा: अभी तक भारत में कोई ठोस Data Protection Law लागू नहीं है।
ग्राफिक्स सुझाव: भारत में 2018–2024 के बीच सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन वाले राज्यों का चार्ट
- मणिपुर: 21 बार
- हरियाणा: 12 बार
- जम्मू-कश्मीर: 12 बार
- राजस्थान: 10 बार
- पश्चिम बंगाल: 9 बार

Source: Indian Express Report (2024)
ALT Text: Chart showing the number of internet shutdowns by Indian states between 2018 and 2024.
IV. सोशल मीडिया और लोकतंत्र: एक दोधारी तलवार
- जहाँ सोशल मीडिया जनता की आवाज़ बन सकता है, वहीं यह फेक न्यूज़ और ट्रोलिंग का माध्यम भी है।
- उदाहरण: 2024 लोकसभा चुनावों में सोशल मीडिया पर 1.2 लाख से अधिक फर्जी पोस्ट चिन्हित की गईं।
- प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी: Facebook, Twitter और YouTube को चुनाव आयोग ने 200 बार नोटिस भेजे।
V. समाधान: लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की रणनीति
1. जवाबदेही और पारदर्शिता
- RTI को सशक्त बनाना, लोकपाल को स्वतंत्र अधिकार देना।
- सांसदों की संपत्ति की सार्वजनिक जानकारी और समय-समय पर ऑडिट।
2. शिक्षा और राजनीतिक साक्षरता
- स्कूल स्तर से नागरिक शास्त्र की गंभीर पढ़ाई।
- कॉलेजों में “यंग पार्लियामेंट” और मॉडल संविधान की अनिवार्यता।
3. मीडिया और सूचना की स्वतंत्रता
- मीडिया को स्वायत्त संस्थानों द्वारा विनियमित किया जाए, न कि सरकार द्वारा।
- डिजिटल मीडिया को भी प्रेस काउंसिल के अंतर्गत लाना।
4. टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पारदर्शिता
- BlockChain आधारित वोटिंग पर रिसर्च और पायलट योजनाएं।
- सरकारी ऐप्स में RTI मॉड्यूल जोड़ना।
5. न्यायपालिका में सुधार
- Fast-track courts की संख्या में 50% वृद्धि।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम की पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
6. नागरिक सहभागिता के नए मॉडल
- जन-सुनवाई ऐप, डिज़िटल जन बजट प्रक्रिया जैसे नवाचार।
- वार्ड स्तर पर मासिक जनमंच कार्यक्रम अनिवार्य बनाना।
VI. निष्कर्ष: लोकतंत्र बचेगा जब हम जागरूक बनेंगे
लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि जीवंत बहसों, आलोचना, सहभागिता और नागरिक चेतना का परिणाम है। अगर हम केवल वोट डालकर मौन हो जाते हैं, तो लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सिमट जाता है।
हमें चाहिए कि:
- हर नागरिक संविधान पढ़े,
- डिजिटल साक्षरता को अपनाए,
- नेताओं से मुद्दों पर जवाब मांगे,
- और फर्जी प्रचार से खुद को बचाए।
क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा कोई और नहीं करेगा — यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।
❝ लोकतंत्र की साँसें ❞
नेताओं के वादे झूठे निकले, जनता फिर भी चुपचाप रही,
मंचों पर भाषण गूंजते रहे, पर रोटी सवालों में कैद रही।
कलम की धार कुंद हुई जब, अख़बार बिकते सत्ता में,
न्याय की कुर्सी देर करे जब, सच्चाई डूबे सत्ता में।
वोट की कीमत भूले सभी, जाति-धर्म में बंट गए,
भीड़ तो दिखी हर रैली में, पर मुद्दे पीछे हट गए।
अब भी समय है जागो सब, सवाल उठाओ खुलकर,
लोकतंत्र तभी बचेगा जब, जनता बो