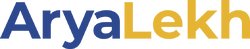उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘स्कूल मर्जर नीति’ को लेकर राज्य भर में असंतोष फैला हुआ है। गांवों में स्थित छोटे सरकारी स्कूलों को एक-दूसरे में समाहित करने की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कई शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
अब जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन याचिकाओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यह ज़रूरी हो गया है कि हम समझें कि यह पूरा विवाद क्या है, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, और क्यों कई ग्रामीण इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं।
याचिकाओं का केंद्रबिंदु क्या है?
याचिकाओं में मुख्य आपत्तियाँ इस प्रकार थीं:
- छात्रों की दूरी बढ़ेगी – छोटे बच्चों को दूरस्थ स्कूलों तक पैदल या असुरक्षित साधनों से जाना पड़ेगा।
- ग्रामीण शिक्षा पर असर – स्कूल बंद होने से गांवों में शिक्षा का माहौल बिखर जाएगा।
- स्थान चयन में पारदर्शिता नहीं – कई अभिभावकों और ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने मर्जर प्रक्रिया में स्थानीय सुझावों की अनदेखी की।
- बिना पूर्व जानकारी के निर्णय – शिक्षकों और ग्रामीण समाज को इस निर्णय की न तो पूर्व सूचना दी गई और न ही उनकी राय ली गई।
सरकार की दलीलें: स्कूल मर्जर क्यों ज़रूरी है?
राज्य सरकार का कहना है कि:
- छात्रों की संख्या बहुत कम है (कई स्कूलों में 10 से भी कम विद्यार्थी हैं), ऐसे में संसाधनों की बर्बादी होती है।
- एकीकृत स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में है।
धरना और प्रदर्शन: मोहनलालगंज बना केंद्र
लखनऊ के मोहनलालगंज में ग्रामीणों ने स्कूल मर्जर के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। प्रधान, अभिभावक और छात्र स्कूल मर्जर को लेकर ADM और जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी ज़ाहिर कर चुके हैं।
“बिना हमसे पूछे हमारे गांव का स्कूल हटा दिया गया, क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है?” – एक स्थानीय अभिभावक

हाईकोर्ट की प्रक्रिया: क्या कहा न्यायालय ने?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि:
- यह एक नीति निर्णय है, लेकिन यदि उसमें प्रक्रिया दोष या मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।
- याचिकाकर्ताओं की दलीलें और सरकार की मंशा, दोनों को संतुलित रूप से देखा जाएगा।
- मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जिससे इस मुद्दे पर सामाजिक विमर्श बना रहे।
गांवों में शिक्षा का भविष्य: मर्जर से लाभ या नुकसान?
लाभ:
✅ एकीकृत संसाधन और शिक्षक
✅ स्मार्ट क्लास और पुस्तकालय की सुविधा
✅ बजट का कुशल उपयोग
नुकसान:
❌ छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी
❌ महिला शिक्षा पर बुरा असर (यातायात सुरक्षा के कारण)
❌ समुदाय का स्कूल से जुड़ाव कमजोर होगा
शिक्षाविदों की राय क्या कहती है?
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मर्जर तभी प्रभावी होगा जब:
- परिवहन की व्यवस्था पुख्ता हो
- पैरेंट्स को विश्वास में लिया जाए
- स्कूल समेकन के बाद सुविधाओं का स्तर बेहतर हो
वरना यह कदम “शिक्षा से दूरी का कारण” भी बन सकता है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: क्या अन्य राज्यों में हुआ ऐसा?
- मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में स्कूल मर्जर की नीतियाँ पहले लागू की जा चुकी हैं।
- जहां कुछ क्षेत्रों में इसका सकारात्मक असर देखा गया, वहीं कई स्थानों पर ग्रामीण विरोध भी सामने आया।
समाज में उठते सवाल: क्या शिक्षा अब सिर्फ आंकड़ों का खेल है?
ग्रामीण लोगों का मानना है कि:
- बच्चों की पहुँच शिक्षा से दूर हो रही है, और यह केवल सरकार की रिपोर्टिंग आसान करने की कवायद है।
- शिक्षकों का स्थानांतरण और अनिश्चितता बढ़ रही है, जिससे शिक्षण गुणवत्ता पर असर पड़ता है।
क्या होना चाहिए अगला कदम?
अब जबकि HC में स्कूल मर्जर से संबंधित याचिकाओं का निर्णय लंबित है, यह जरूरी है कि:
- सरकार नीति में लचीलापन और संवाद लाए।
- स्थानीय समाज, शिक्षक और अभिभावकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए।
- हर स्कूल के संदर्भ में अलग दृष्टिकोण अपनाया जाए – “One Policy Fits All” नहीं चलेगा।
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रैली 2025: क्या यह ऐतिहासिक गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति बदल देगा?
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का सच: गरीबी, नीति और संघर्ष के बीच दम तोड़ते सपने